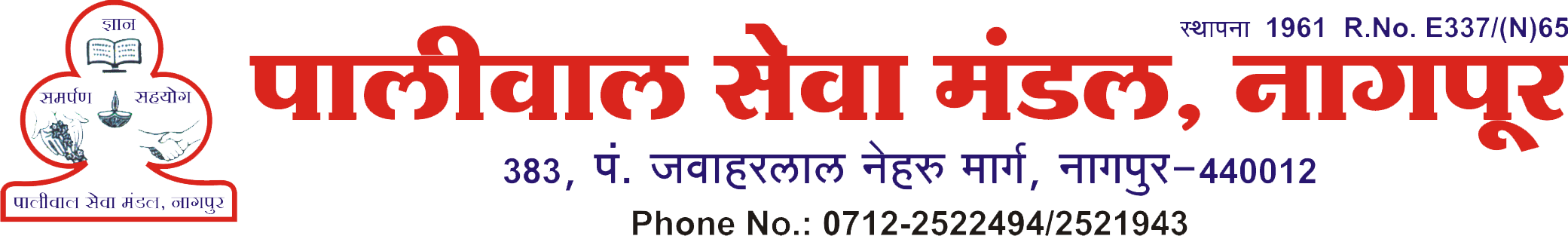“पालीवाल ब्राह्मण” - इतिहास
पालीवाल सेवा मंडल एक समर्पित सामुदायिक संगठन है, जो पालीवाल समाज को सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक उत्थान और शैक्षणिक समर्थन के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए कार्यरत है।
( यह लेख “पालीवाल ब्राह्मण” किताब, लेखक श्री ओमप्रकाश पालीवाल I.E.S(Retd.)(M.A. LLB) ३२७८ सेक्टर 15D Chandigarh द्वारा मार्च २००५ को प्रकाशित )
पालीवाल - इतिहास के लेखक पं. शिवनारायण पालीवाल के अनुसार मंडोवर (वर्तमान जोधपुर के निकट स्थित) के पड़िहार वंशीय महाराज लक्ष्मणराव ने विक्रम सम्वत् 534 में अपने वसिष्ठ गोत्री ब्राह्मण गुरु को पाली का संकल्प करके एक दान पत्र लिख दिया। तब से ब्राह्मणों का वह वंश जिसको पाली दान में मिली थी, पाली में आकर बस गया। उसके वहां आ बसने से उसके दूसरे गोत्री भाई तथा रिश्तेदार भी आकर बसने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे इसमें एक लाख घर बाह्मणों के हो गए और पाली इनका शासनीय (स्वतंत्र) गांव हो गया। इसमें पालीवालों का रहना सभी इतिहासकारों ने माना है।
इस संदर्भ में स्वतंत्र का अर्थ केवल यही है कि पाली को भू-राजस्व एवं अन्य कर राज्य को नहीं देने पड़ते थे। पाली प्रारम्भमें पड़िहारों के आश्रित रहा, फिर कभी परमार, कभी सोलंकी, कभी चालुक्य, कभी चौहानों के संरक्षण में रहा। धीरे धीरे पाली नगर की उन्नति हुई। यहां के निवासियों ने इसे व्यापारिक केन्द्र बना दिया। इसका मांडवी और खम्भात के बंदरगाहों द्वारा आफ्रिका , अरब, ईरान आदि देशों से माल मंगवाने और भेजने का सीधा संबंध था। मारवाड़ के चार प्रसिद्ध नगरों मंडोर, पाली, सोजात, जैतरन में इसकी गिनती होने लगी।
उत्थान के बाद पतन प्राकृतिक नियम है। पाली भी इससे न बच सकी। इसके धनिक वर्ग पर सभी की दृष्टि लगी रही और कई बार पाली को आततायियों ने लूटा। परन्तु हमें वह वर्ष ढूंढना है जिसमें लुटकर हम पाली को छोड़ आए। इस संबंध में विभिन्न मतों की समीक्षा निम्न है।

-
पालीवाल भाटों का मत
हमारे भाटों के अनुसार विक्रम की बारहवीं सदी तक ही पाली के शासनकर्ता पालीवाल ब्राह्मण रहे हैं। विक्रमी संवत् 1148 की श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मुहम्मद ग़ौरी नामक बादशाह ने चढाई करके इनसे पाली छीन ली। परन्तु इतिहास ग्रन्थों से यह बात निर्मल सिद्ध होती है।
तबकात-ए-नासिरी तथा "तारीख-ए-फ़रिश्ता" (इतिहास ग्रन्थ है जो फारसी भाषा में है ) के अनुसार मुइजुद्दीन घुरी (मुहम्मद ग़ौरी) ने सन् 1178 (विक्रमी सम्वत् 1235) में गुजरात पर चढ़ाई की। वह किराड, नाडोल होता हुआ माउन्ट आबू तक पहुंचा। कयाद्रा नामक स्थान पर युद्ध हुआ और उसकी हार हुई। परन्तु वह किसी प्रकार वहां से सेना समेत भागने में सफल हुआ।
इस प्रकार विक्रमी सम्वत् 1148 में हमारा पाली छोड़ना सिद्ध नहीं होता। परन्तु हमारा श्रावणी का न मनाना हमारे भाटों के इस मत की पुष्टि करता है कि पाली का पतन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हुआ परन्तु वह श्रावणी विक्रमी सम्वत् 1148 की नहीं किसी अन्य सम्वत् की है।
-
कर्नल टाड का मत
कर्नल टाड का 'राजस्थान इतिहास' एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। टाड के अनुसार सन् 1156 में पालीवालों पर एक भारी विपत्ति पड़ी। इन्हें 'अरावली' पर्वत श्रेणी में रहने वाले मीने मीर आदि सताया करते थे। इनसे रक्षा पाने के लिए पाली के ब्राह्मणों ने कन्नोज के राजकुमार सीहाजी से प्रार्थना की जो द्वारका से तीर्थ यात्रा करके पाली से लोट रहे थे। सीहा जी ने उनकी रक्षा की परन्तु राज्य प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर न चूकने में उन्होंने अपनी भलाई समझी और होली के दिन प्रमुख ब्राह्मणों का वध करके पाली को उनसे छीन लिया।
परन्तु आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार सीहा जी ने सन् 1243 के लगभग पाली के समीपवर्ती स्थानों पर विजय प्राप्त करके वहां राठोड़ वंश की नींव डाली है। बीठू में पाए गए शिलालेख से सीहा जी की मृत्यु सन् 1273 (सम्वत् 1330 विक्रमी) में हुई है। अमिया ढाढीकृत 'पालीवाल जस प्रकाश' में सीहा जी का सम्वत् 1292 विक्रमी में पाली आना लिखा है। छब्बीस वर्ष तक सुख पूर्वक वहां रहना लिखा है, फिर बारह वर्षों तक युद्ध में रहना। इस प्रकार सम्वत् 1330 में वीरगति पाना लिखा है। शिलालेख कर्नल टाड के मत की अपेक्षा इतिहास का ठोस स्तोत्र है। अतः सीहा जी 1156 सन में पाली का शासक सिद्ध नहीं होता क्योंकि 1273 और 1156 में 117 वर्ष का अंतर है और मनुष्य की औसत आयु इससे कम होती है।
-
अन्य ग्रन्थकारों का मत
कुछ ग्रन्थों में दिल्ली के शासक फीरोजशाह का नाम पाली के तोडने वालों में लिखा पाया जाता है। दिल्ली सल्तनत के जमाने में फीरोजशाह नाम के तीन बादशाह हुए हैं। एक गुलाम वंश में, दूसरा खल्जी वंश में और तीसरा तुगलक वंश में।
- गुलामवंशीय बादशाह का पूरा नाम रूकनुद्दीन फीरोजशाह था। यह 21 अप्रैल 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और केवल 6 मास 28 दिन शासन करके 19 नवम्बर 1236 को कत्ल कर दिया गया। इसने कहीं पर भी आक्रमण नहीं किया।
- खल्ज़ी वंशीय जलालुद्दीन फीरोजशाह ने जून, 1290 में शासन संभाला। इसने राजस्थान पर आक्रमण किया। शाही सेना रिवाड़ी, नारनौल होती हुई अलवर पहुंची और मंडावर को जीत लिया। फिर झेन पर आक्रमण करके वहां के दुर्ग को जीत लिया और उसे विध्वंस कर डाला। उसके उपरांत रणथंभौर का घेरा डाला परन्तु उसे विजय किए बिना ही फीरोजशाह दिल्ली वापिस आ गया। कुछ इतिहासकार इसे मारवाड़ स्थित मंडोर पर आक्रमण बताते हैं और इसी आधार पर पं. शिवनारायण जी ने 'पालीवाल इतिहास' (पृष्ठ 89) में लिखा है। 'अगर पाली को फीरोजशाह ने तोड़ा है तो सीहा जी की मृत्यु के बाद में टूटी है और इसके टूटने का समय सम्वत् 1346 के लगभग मानना पड़ेगा' । परन्तु मान्य ग्रन्थों के आधार पर इसे शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मंडावर ही मानना पड़ेगा। एक ख्यात के अनुसार फीरोजशाह बादशाह मक्का की यात्रा करते समय पाली में रूका और पालीवालों के धन को लूटा। यह समाचार सुनकर आस्थान जी ने खेड से आकर बादशाह से युद्ध करके लूट का धन वापिस लिया और पाली की घेराबंदी भी समाप्त करा दी। आस्थान की मृत्यु तुर्कों से युद्ध करते हुए सन् 1291 विक्रमी सम्वत् 1348 में मानते हैं। इस प्रकार सम्वत् 1348 तक पाली में हम रहते थे।
- तीसरा फीरोजशाह तुगलकवंश में हुआ इसने राजपूताने के किसी भी भाग पर हमला नहीं किया।
-
स्वकीय मत
मेरे विचार के अनुसार अलाउद्दीन खल्ज़ी ने अपने लिवाना अभियान में सन् 1309 में पाली को लूटकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस संबंध में मेरा विश्लेषण निम्न है-
- पाली कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था जिसकी विजय का वर्णन इतिहास में अन्य राज्यों की भांति होता। पं. शिवनारायण जी के अनुसार पाली उस समय जालोर में था अतः जालोर पतन से पाली पतन स्वतः सिद्ध होता है। 'तारीख - ए - मुबारकशाही' (पृष्ठ 78) के अनुसार जालोर का पतन भी सिवाना विजय के वर्ष में हुआ। हिजरी सन् 708 का समय 21 जून 1309 से 10 जून 1310 तक है। अतः इसके मध्य ही जालोर का पतन हुआ।
- अलाउद्दीन की देवगिरी, वारंगल आदि लूटें इस बात का प्रमाण हैं कि उसका धनी नगरों को लूटकर नष्ट करने का स्वभाव था। पाली के वैभव का उसके सेनापतियों को गुजरात विजय (सन् 1299) में ज्ञान हो ही गया था। अतः पाली की सम्पन्नता ने सुल्तान का ध्यान आकर्षित किया। सिवाना जाने में पाली मार्ग में ही पड़ता था। इसलिए इसकी घेराबंदी करके इसको लूटा और पूर्ण रूप से विध्वंस करके सिवाना की ओर बढ़ा।
- सिवाना अभियान के लिए शाही सेना ने सुल्तान की अध्यक्षता में बुधवार 3 जुलाई, 1309 (13) मुहर्रम, 708 हिजरी सन् को प्रस्थान किया और 9 सितम्बर, 1309 के दिन सिवाना पर विजय प्राप्त की। (A Comprehensive History of India, Volume Five, The Delhi Sultanat, Page 396).
- हमें इस अभियान की तारीखों से विक्रम सम्वत् श्रावण के चान्द्र मासों और हिजरी सन् के चान्द्र मासों में काफी साम्यता मास, पूर्णिमा तिथि तथा उसके वार को जानना है। विक्रम सम्वत् है। हिजरी सन् का चान्द्र मास अमावस्या के उपरांत चंद्र दर्शन से प्रारम्भ होता है परन्तु व्यवहार में मुसलिम मास की पहली तारीख चन्द्र दर्शन के दसरे दिन लिखी जाती है। विक्रम मास अमावस्या के अगले दिन से प्रारम्भ होता है। चन्द्र की गति एक समान नहीं इसी कारण चान्द्र मास का मान 28 से 31 दिन तक हो जाता है, परन्तु हिजरी मास में इसका मान 29 या 30 दिन होता है। इस कारण एक दिन का अंतर साधारणतया दोनों मासों में संभव है। 3 जुलाई, 1309 को 13 मुहर्रम होने से पहली मुहर्रम 21 जून, 1309 को बैठती है। विक्रम सम्वत् 2050 में हिजरी सन् 1414 का प्रारम्भ-पहली मुहर्रम - 22 जून सन् 1993 से हुआ। इस वर्ष श्रावणी 2 अगस्त 1993 की थी। स्थूल गणित से सन् 1309 में श्रावणी 1 अगस्त को पड़ती है। परन्तु अंतिम निर्णय देने से पहले यह भी देखना होगा कि इन दोनों वर्षों में अधिक मास था या नहीं। सम्वत् 2050 में भाद्रपद अधिक मास था। सन् 1309 में विक्रमी सम्वत् 1366 था। पंचांग गणित के अनुसार भाद्रपद 19 वर्ष बाद अधिक मास होता है। इस गणित से सम्वत् 1366 में भी भाद्रपद अधिक मास था। इस प्रकार संवत् 1366 और संवत् 2050 में काफी साम्यता है और स्थूल गणित से 1 अगस्त, 1309 को श्रावणी पड़ती है परन्तु उस दिन गुरुवार था। हमारी मान्यता बुधवार की है। ऊपर बताया जा चुका है कि औसत मास और सूक्ष्म स्पष्ट मास में एक दिन का अंतर साधारणतया होता है। इससे विक्रम संवत् 1366 की श्रावण शुक्ल पूर्णिमा बुधवार को होने की पूर्ण संभावना है जिस दिन 31 जुलाई, 1309 थी। अतः पाली का पतन विक्रम संवत् 1366, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा बुधवार का मानना तर्कपूर्ण एवं युक्ति संगत है।
-
गौड़ ब्राह्मण से पालीवाल ब्राह्मण
भविष्य पुराण' के अनुसार सरस्वती और दृषद्वती (वर्तमान घग्घर) इन दो देव नदियों के बीच के देश को ब्रह्मावर्त कहते हैं। श्री परमेश्वराचार्य के अनुसार ये ब्राह्मण सबसे पहले ब्रह्म क्षेत्र - गौड़ देश में जाकर तपस्या करने लगे और सदाचार में प्रवृत होकर सबके सब वेदों के पठन पाठन में लगे। ब्रह्म क्षेत्र में रहने वाले उन ब्राह्मणों की संज्ञा गौड़ हो गई। फिर उन्हीं ब्राह्मणों के फट कर दस प्रकार के ब्राह्मण हो गए। विन्ध्य पर्वत से उत्तर क्षेत्र में रहने वाले पंच-गौड़ तथा उससे दक्षिण में रहने वाले पंच द्राविड़। आगे चलकर इनके अनेक भेद हो गए। इनकी संख्या 1444 ग्रन्थकार ने बताई है। ये भेद इनके देश देशान्तरों में बसने से हुए। कुछ के नाम उनके निवास स्थान के निकास से पड़ गए। पालीवाल नाम भी पाली से निकास के कारण पड़ा। यथा- 'खंडेलवाल ग्रामाश्च, भार्गवाश्च मरूस्थला। पल्लीस्था शंखवासाश्च धन्वा पांचाल वासिनः ।।' पं० हरिकृष्ण जी व्यंकटराव शास्त्री ने अपने 'बृहज्ज्योतिषार्णव ग्रन्थ' में पालीवाल ब्राह्मणों को गौड़ ब्राह्मणों की एक मुख्य शाखा माना है।
उनके अनुसार पल्लीवाल ब्राह्मण पल्ली - पाली - नामक ग्राम से निकले हुए हैं, ये सब मारवाड़ में रहते हैं और विशेषतया वैश्य कर्म किया करते हैं। फिर भी ब्राह्मणों के छः कर्मों में से एक कर्म इन लोगों में अभी तक विशेष रूप से चला आता है। ये लोग मंदिर और विष्णुयाग (यज्ञ) बड़ी विधिपूर्वक कराते हैं। पं० छोटेलाल शर्मा ने अपने 'ब्राह्मण जाति निर्णय' ग्रन्थ (पृष्ठ 339) में पालीवाल ब्राह्मणों की चर्चा करते हुए लिखा है -
मारवाड़ की जातीय रिपोर्ट में लिखा है- 'पालीवाल गौड ब्राह्मणों में से निकले हुए ब्राह्मण हैं। इनका निकास पाली से होने के कारण बाहर ये लोग पालीवाल कहे जाते हैं।' मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मुंशी देवीप्रशाद, महकमा इतिहास, राज मारवाड़, अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 116 में लिखते हैं- 'पाली बहुत पुराना शहर है ......यह शहर पालीवाल ब्राह्मणों का वतन है।' मूता नेनसी अपनी 'ख्यात' में पालीवालों को ब्राह्मण कहते हुए लिखते हैं- 'आसथान जी डैरो पाली रे ब्राह्मण (पल्लीवाल) - रे घरे कीनो' विदेशी लेखकों में कर्नल टाड, विलसन आदि ने भी पालीवालों को ब्राह्मण ही कहा है। आधुनिक इतिहासकारों ने भी पाली में बसे ब्राह्मणों को पालीवाल ब्राह्मण कहा है।
"Pali was then an opulent and prosperous city inhabited by Pallival Brahmans." (A Comprehensive History of India-Vol. 5. The Delhi Sultanat by M. Habib and K.A. Nizami. page 809).
पाली छोड़ने के बाद ही हम पालीवाल ब्राह्मण कहलाए।
-
गोत्र प्रवर
गोत्र प्रवर का सम्बन्ध मानव सृष्टि के साथ है। सृष्टि के आदिकर्ता ब्रह्मा जी अपनी तपस्या द्वारा सुष्टि वर्धन में प्रवृत होते हैं। अपने मानसिक संकल्प से 9 मानस पुत्रों को जन्म देते हैं जो भृगु, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वसिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु और दक्ष हैं। इन ऋषियों से ही गोत्र प्रवर का प्रारम्भ होता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक मन्वन्तर के सप्तर्षि भी उस मन्वन्तर के गोत्रकार ऋषि माने जाते हैं। इस समय श्वेत वाराह कल्प का सातवा मन्वन्तर- वैवस्वत चल रहा है। इस मन्वन्तर के सप्तर्षि - विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ तथा कश्यप हैं। इनमें जमदग्नि भृगुवंशी, भरद्वाज तथा गौतम अंगिरा वंशी, कश्यप मरीचि के पुत्र तथा विश्वामित्र को अत्रिवंश की शाखा में माना जाता है। क्रतु संतानहीन हो गए तो उन्होंने अगस्त के धर्मज्ञ पुत्र इध्मवाह को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। पुलह का मन अपनी संतान को देखकर प्रसन्न नहीं रहता था। अतः उन्होंने अगस्त के पुत्र दृढ़ास्य को पुत्र रूप में वरण कर लिया। पुलस्त्य ऋषि ने अपनी संतति को राक्षसों से उत्पन्न होते देखकर अगस्त के ही अन्य पुत्र को पुत्र रूप में वरण कर लिया। इस प्रकार अगस्त्य वंश भी गोत्रकार ऋषियों के वंश में हुआ। इन ऋषियों की पौत्रादिक संतान का ही गोत्र शब्द से ग्रहण होता होता है। इसको पाणिनि ने 'पौत्र प्रभृति गोत्रम्' सूत्र में कहा है। वास्तव में जिन पौत्रादिकों द्वारा अपने पूर्वजों का ज्ञान होता है वही गोत्र है।
गोत्र दो प्रकार से होते हैं। ब्राह्मणों में यौन संबंध से और क्षत्रिय, वैश्यों में विद्या संबंध से होते हैं। पाणिनि ने कहा है 'विद्या योनि सम्बन्धेभ्यो'।
-
प्रवर
प्रवर शब्द कई अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ के अनुसार वंश का मूल-पूर्वज प्रवर कहलाता है। इसके अनुसार सभी वंशों के मूल - पूर्वज अपने अपने गोत्र के तथा अपने वंश में अन्य गोत्रकार ऋषियों के भी प्रवर होते हैं। दूसरे अर्थ में वंश में जो विशेष गुण सम्पन्न ऋषि हुए हैं उन्हें भी प्रवर माना गया है। 'शतपथ ब्राह्मण' में पिता, पितामह तथा प्रपितामाह को प्रवर माना गया है। तीसरे अर्थ में, गोत्रकार ऋषि के यज्ञ में जिन अन्य ऋषियों की भी सहायता ली जाती थी उन्हें भी प्रवर ही कहा जाता था। एक गोत्र के प्रवर अधिक से अधिक 5 ही होते हैं।
पहले कुल परम्परा से अविच्छिन्न प्रवरों द्वारा गोत्र का निर्णय किया जाता था क्योंकि प्रवर की एकता से ही गोत्र की समता होती है 'परक्यात गोत्रस्यैकत्वमिति’ । इसका ही विवाहादि से विचार किया जाता था। जिन गोत्रों के एक ही प्रवर होते थे उन गोत्रों में परस्पर विवाह वर्जित था 'परस्परमवैवाद्या ऋषयः परिकीर्तिता'।
-
पालीवालों के गोत्र/प्रवर
पाली छोडने के कुछ दिनों बाद गिनती करने पर ज्ञात हुआ कि बचे हुए ब्राह्मण 12 गोत्रों के थे। इनमें से 4 गोत्र भरद्वाज, वामदेव, वैन्य और कौशिक - आवासादि की खोज में गुजरात की कि ओर चले गए। शेष 8 गोत्र- वसिष्ठ, गर्ग, पराशर, मुद्रङ्गल, जातुकर्ण, उपमन्यु, शाण्डिल्य और कोण्डिन्य प्रारम्भ में जैलसमेर राज्य में गए और वहां अपने 84 गांव बसाए। बाद में वहां से चलकर जोधपुर, बीकानेर राज्यों में बसे। उसके पश्चात् गत तीन शताब्दी में वहां से चलकर आजीविका की खोज में भारत के अन्य राज्यों में जा बसे। आज उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बसे हैं। नौकरी करने वाले तो अन्य राज्यों में भी है। भारत के कुछ नगरों में बसे पालीवाल के गोत्रों में अत्रि गोत्र भी पाया गया है। इस प्रकार 9 गोत्र हैं।
-
प्रवर
मत्स्य पुराण के अनुसार उपरोक्त गोत्रों के प्रवर निम्न कोष्टक में दिए हैं।
गोत्रों के खाप/नख/अल्ल
पाली छोड़ने के पश्चात् हमारे पूर्वज सर्वप्रथम जैसलमेर राज्य में गए और वहां पर अपने 84 खेड़े बसाए। इन खेड़ों को उन्होंने अपने नाम से बसाया। जिस व्यक्ति ने जो गांव बसाय कालान्तर में उसके वंशजों ने उस नाम को भी अपने साथ जोड लिया। पूर्वज के इस नाम को ही खाप, नख या अल्ल कहते है जो निम्न हैं।
पालीवालों के गोत्र, प्रवर, खाप आदि कोष्टक
# गोत्र प्रवर खाप/नख 1 वसिष्ठ वसिष्ठ मुंधा, रत्ता, खीमल, मूला, टीकमिया, हुलकाड़िया 2 गर्ग अंगिरा, बृहस्पति, भरद्वाज, गर्ग, सैत्य हरजाल, बुणिया, छिरक, जगिया, जाजिया, जस्सू, गेजड, जग्गा, कंवरा, कडवा, दुलिया, मूणपिया, हरदावल, मोढ़ा, हर्षण 3 पराशर वसिष्ठ, पराशर, शक्ति पुनद, साधू, घड़िया, मूलदेव, चौधरी, आसदेव, बग्घन, बीसल, माधव, सोमेरी, हड्डा, जस्सू, राणा, खीडल, देवडराणा, मारद, नोता, भर्मा 4 मुदगल अंगिरा, मत्स्यदग्ध, मुद्गल पित्थड धामट, कुलधर, सारण, तेजड, बुट्टर, चंदन, भायल, धुलिया, निमिया, दामोदर, गुरेरिया, देढ़ा, रिद्धू,भीमसरिया, मोकल, पाटोलिया, तेमा 5 जातुकर्ण वसिष्ठ, अत्रि, जातुकर्ण ढ़ीयाँ, ठोमा 6 उपमन्यु वसिष्ठ, इन्द्रप्रमति, भगीवसु सुहाम 7 शाण्डिल्य असित, देवल, कश्यप सूरा 8 कोण्डिन्य (कुण्डिन) वसिष्ठ, कुण्डिन मित्रावरूण, जानड़ 9 अत्रि श्यावाश्व, अत्रि, आर्चनानश ---- -
पालीवालों का वेद (शुक्ल यजुर्वेद)
गोत्रकार ऋषि के यहां परम्परा से जिस वेद का पठन-पाठन अविच्छिन्न रूप से चला आता हो वही उस गोत्र का वेद है। हमारे 9 गोत्रों में केवल शाण्डिल्य गोत्र का वेद सामवेद है। शेष 8 गोत्रों का वेद शुक्ल यजुर्वेद है।
-
शाखा (माध्यन्दिन)
शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं हैं जिनमें हमारी माध्यन्दिनीय शाखा है।
-
वाजसनेयि - माध्यन्दिन संहिता
इसका विभाग अध्यायों तथा कण्डिकाओं में है। इसमें 40 अध्याय तथा 1975 कण्डिकाएँ है। कण्डिकाओं में मंत्रो का विभाजन है। इस संहिता के प्रथम 39 अध्यायों में श्रौत कर्मकाण्ड है। जिसके अन्तर्गत दर्श- पूर्णमास, पिण्ड- पितृ यज्ञ, अग्निहोत्र, राजसूय याग, वाजपेय याग, शतरूद्रिय होम के मंत्र वसोर्धारा - मन्त्र, सौत्रामणी याग, अश्वमेध यज्ञ, पुरूष मेध, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, शिवसङ्कल्पोपनिषद्, पितृमेध तथा प्रवर्ग्य विषयक मंत्र हैं। चालीसवें अध्याय में ईशावास्योपनिषद् है।
-
शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण
माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण में 14 काण्ड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण तथा 7624 कण्डिकाएँ हैं। शत अध्याय होने के कारण इसका शतपथ नाम सार्थक है। इस शतपथा ब्राह्मण में प्रथम काण्ड से लेकर अंतिम काण्ड तक विषयों का क्रम माध्यन्दिन संहिता के अनुसार ही है। एक अपवाद पिण्ड पितृयज्ञ है जिसका वर्णन संहिता में दर्शपूर्णमास के अनन्तर है परन्तु ब्राह्मण में आधान के अनन्तर।
-
आरण्यक (बृहदारण्यक)
शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मणों का आरण्यक ग्रन्थ बृहदारण्यक है और इसके प्रवचनकर्ता आचार्य भी महर्षि याज्ञवल्क्य हैं।
-
उपनिषद्
शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध 19 उपनिषद् हैं जिनमें प्रमुख ईशावास्योपनिषद् तथा बृहदारण्यकोपनिषद् हैं।
-
श्रौत सूत्र
शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन श्रौत सूत्र है।,
-
गृह्य सूत्र
शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर गृह्य सूत्र है। कात्यायन श्राद्ध सूत्र है।
-
धर्म सूत्र
याज्ञवल्क्य स्मृति है।
-
पालीवाल ब्राह्मण की बारह छेड़ और उनके गांव
पाली पतन के पश्चात् हमारे पूर्वजों ने पाली को छोड़ दिया और आवास तथा व्यवसाय की खोज में वहां से कई टोलियों में निकल पड़े। उनमें से एक टोली ने जैसलमेर की ओर प्रस्थान किया। इस टोली का प्रथम मुकाम ओला पर हुआ जहां इनके यज्ञ स्तम्भ अभी तक वर्तमान हैं। पण्डित शिव नारायण जी के अनुसार 'ये स्तम्भ ओले के खेतों में अभी तक गडे हुए हैं और पालीवालों के यज्ञ स्तम्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं'। फिर ये बरयाडे की तरफ बढ़े और वहाँ पर कुछ दिन रहे। जैसलमेर में इन्होंने पांच क्षेत्रों में निवास किया और प्रत्येक क्षेत्र में अपने गांव बसाकर रहे।
(क) जैसलमेर की पाँच छेड़
-
बरियाड़ा और कोटड़ा
पण्डित शिवनारायण जी के अनुसार बरियाड़ा एक झील का नाम है जो बाड़मेर स्टेशन से करीब 32 कोस पश्चिम दिशा में है। इसके चारों तरफ छोटी-छोटी पहाड़ियां है। पहाड़ियों से घिरे हुए इस हिस्से का नाम बरियाड़ा है।
कोटड़ा एक जागीर का ठिकाना है जो अब जोधपुर में है, परन्तु पालीवालों की छेड़ों के हिसाब से इसके 24 गांव जैसलमेर की छेड़ में गिने जाते हैं।
कोटड़ा छेड़ के गांव
- 1. गूंगा 2. जसेरो गांव 3. नेगडरो 4. मड़ाई 5. मत्तीरोगोल 6. राजडावल 7. खोड़ाल 8. साँधू 9. कौडियासर 10. सान्डा 11. डाँगरी 12. बीजोराई 13. भींयासर 14. रेवड़ी 15. कोठाबड़ा 16. कोठाछोटा 17. काठोड़ा 18. सीतोडाई 19. जसू आ 20. मंडा 21. दईकोट 22. बोंडा 23. रौंडी 24. मोढ़ा
-
नेवाण
पण्डित शिवनारायण जी के अनुसार नेवाण का अर्थ नीचाई की जमीन है। यह एक 25-30 कोस का लंबा चौड़ा जमीन का हिस्सा बरियाड़े और बुजंकठे की पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। इस हिस्से में बसे हुए नौ खेड़ों को नेवाण के नौ खेड़े कहते हैं।
नेवाण छेड़ के गांव
- 1. नेडिया 2. पीथोडाई 3. भू 4. धन्वा 5. पीपलड़ा 6. गुरेरा छोटा 7. गुरेरा बड़ा 8. बासनपी छोटी 9. बासनपी बड़ी
-
बुजकंठा
पण्डित शिवनारायण जी के अनुसार बुजकी खडीन के आसपास की पहाड़ियों पर पालीवालों के बारह खेड़े बसे हुए थे। परन्तु अपनी पुस्तक में उन्होंने केवल 10 गांवों के नाम दिए हैं।
बुजकंठा छेड़ के गांव
- 1. कुलधर 2. जाजिया 3. देढ़ा 7. दामोदर 5. धुल्या 6. निमिया 4. खावा 8. मूणपिया 9. रिध्दु 10. कँवरा
-
खडाल
पण्डित शिवनारायण जी के अनुसार जैसलमेर के उत्तरीय भाग की भूमि के थोड़े से हिस्से को खडाल कहते हैं। इसके अधिकांश भाग में पथरीली जमीन है। इस भाग का क्षेत्रफल सौ वर्ग मील से ज्यादा नहीं है। इस क्षेत्र में पालीवालों के 24 खेड़े थे परन्तु पंडित शिवनारायण जी ने निम्न 20 खेड़े दिए हैं।
खडाल छेड़ के गांव
- 1. काठोड़ी 2. नाणेला 3. खींया 4. खींवलसर 5. जसूआ 6. जग्गा 7. रत्ता 8. नेडाई 9. मुन्धा 10. जानड़ 11. धामट 12. घड़िया 13. हड्डा 14. राणा 15. जस्सुराणा 16. बीसल 17. आसदेव 18. माधो 19. चौधरी 20. मूलदेव
-
विक्रमपुर
यह मारवाड़ के प्राचीन कोटों में से एक है। इसमें पालीवालों के 15 खेडे थे। परन्तु 'पालीवाल इतिहास' में निम्न 12 खेडे दिए हैं।
विक्रमपुर छेड़ के गांव
- 1. बाप 2. भोजा की बाप 3. बावड़ी 4. सर (बुणियासर) 5. बधाउड़ा 6. माणकसर 7. पुन्धा 8. ढींया 9. सेवड़ा 10. नवा तालाब 11. बड़ी जौंध 12. छोटी जौंध
(ख) मारवाड़ (जोधपुर) की छः छेड़
-
पोकरण
पोकरण जोधपुर का एक कस्बा है। इसमें पालीवालों के 19 गांव हैं।
पोकरण छेड़ के गांव
- 1. उगरास गुन्धा 2. उगरास कर्माणी 3. लऊवाँ 4. लाठी 5. ओढ़ाणियाँ 6. चाचा 7. धूलसर 8. बड़ली 9. मड़ला पुन्सी का 10. भुणियाणा 11. मावा 12. ढढू 13. मड़ला बड़ा 14. काला 15. झलारिया 16. फल सूंड 17. भीयांड 18. चांसवा
-
फलौदी
फलौदी भी जोधपुर का एक परगना है। इसमें पालीवालों के 17 खेड़े हैं।
फलौदी छेड़ के गांव
- 1. सांवरींज 2. दयाकोर 3. छीला 4. जालोड़ा 5. होपारड़ी 6. मोखेरी 7. बारणाऊ 8. भोजाकोर 9. भाखरी 10. गोदड़ली 11. बिटड़ी 12. निन्नेऊ 13. बावड़ी 14. बनासर 15. आमला 16. बावणू 17. मयाकोर
-
कोरणावटी
कोरणावटी एक ठिकाना था जिसके नाम पर इस क्षेत्र को ही कोरणावटी कहते हैं। पालीवालों के 24 खेड़े इस क्षेत्र में थे जिन्हे कोरणावटी की छेड़ कहकर पुकारा जाता है। परन्तु 'पालीवाल - इतिहास' में केवल 19 ही दिए हैं।
कोरणावटी छेड़ के गांव
- 1. नेवरी 2. मूणपुरा 3. मड़ली 4. बघनावास 5. पतारखेड़ा 6. रोड़वा बड़ा 7. रोड़वा छोटा 8. कुई 9. गंगावा 10. परालिया 11. सूराणी 12. दूगर 13. भाटेलाई 14. तुलेसर 15. बावड़ली 16. लोरड़ी 17. चिड़वाई 18. चेराई 19. गागाडी
-
मालाणी
यह उस क्षेत्र का नाम है जो जोधपुर के पश्चिमी भाग में सिन्ध और जैसलमेर की सीमा पर स्थित है। पण्डित शिवनारायण जी के अनुसार इस प्रदेश में पालीवालों के 12 खेड़े हैं जिनको मालाणी में होने की वजह से मालाणी की छेड़ कहते हैं।
मालाणी छेड़ के गांव
- 1. जसोल 2. तेमावास 3. सोमावास 4. बजावास 5. सरली 6. तलवाड़ा 7. बोरावास 8. मोढावास 9. खेड 10. जेरडा
-
सेवाणची
सिवाणा जोधपुर से लगभग 50 मील नैऋत्य कोण में स्थित है। पण्डित शिवनारायण जी के अनुसार इसमें पालीवालों के 12 खेडे थे। इन खेडों को सिवाणा क्षेत्र में होने की वजह से सेवाणची की छेड़ कहते हैं।
सेवाणची छेड़ के गांव
- 1. बालोतरा 2. पचपदरा 3. चिडानी 4. मड़ापड़ा 5. गोपड़ी 6. रामीण 7. मूंगड़ा 8. बीठूजा 9. भांडिया वास 10. कुड़ी 11. नेवाई 12. ऊमरलाई
-
गोड़वाड़
जिस प्रदेश में पालीवालों के ये खेड़े हैं उसको प्राचीन समय से ही गोड़वाड़ कहते हैं। पंडित शिवनारायण जी के अनुसार पालीवालों ने इधर अपने खेड़े विक्रम की सोलवीं सदी के आखिरी समय से बसाने प्रारम्भ किए और अठारवीं सदी तक बराबर बसाते रहे। ये गिनती में साठ थे। परन्तु 'पालीवाल इतिहास' में केवल 34 ही दिए हैं।
गोड़वाड़ छेड़ के गांव
- 1. काकेलाव 2. जाजियाल 3. बेंनण 4. बीसलपुर 5. वीडाव 6. लोलाव 7. भाटिण्डा 8. पोटालिया 9. चौंदासणी 10. सऊपुरा 11. बिजपड़ 12. खांवल 13. भांगेर 14. नींवली 15. निम्बाड़ा 16. खारावेरा भींवतो का 17. वाणियावास 18. विरामी 19. राजपुरिया 20. आंटड 21. मोडी जोशियों की 22. खेजडली 23. दूधिया 24. श्रींतड़ा 25. मडपुरिया 26. चुलेलाई 27. मूंगलो 28. नीमली बुट्टों की 29. खारावेरा पुरोहितों का 30. डूंडड़ी 31. वागड़िया 32. कानाव 33. बोंडाई 34. खारड़ा
(ग) बीकानेर की छेड़
इसमें पालीवालों के 13 खेड़े हैं। इन्हीं खेड़ों को बीकानेर की छेड़ तथा इसमें रहने वाले पालीवालों को बीका कहकर पुकारते हैं।
-
बीकानेर छेड़ के गांव
- 1. चाँडासर 2. कोटड़ी 3. मढ़ 4. डेहा 5. गुडा 6. दयात्रा 7.झज्जू 8. नैणिया 9. मोरवा 10. भायला 11. हाडला 12. चानी 13. भोजुसर
-
बरियाड़ा और कोटड़ा
-
पालीवाल शिलालेख
शिलालेख इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे जैसलमेर पुर, बीकानेर में 240 गांव हैं परन्तु 'पालीवाल शिलालेख संग्रह' में 148 गांवों में प्राप्त शिलालेखों का अधूरा वर्णन है। पण्डित शिवनारायण है के अनुसार हमने जो शिला लेख संग्रह किए हैं वे आधे भी नहीं है। 'खर्च की कमी के कारण गांवों के अन्दर के समस्त शिलालेखों को भी हम यथावत् संग्रह न कर सके।' इन गांवों में संग्रहित 889 शिलालेखों में 220 देवली, 282 छतरी, 121 चबूतरे दो डोली, तीन धर्मशाला एवं 10 चौकी उजाणे की हैं। जेए 251 शिलालेखों का विवरण निम्न कोष्टक में दिया है: -
छेड़वार संग्रहित शिलालेख कोष्टक
शिलालेख संख्या
# छेड़ का नाम गांव संख्या मंदिर कूप / तालाब सती जुझार झोंवर योग 1 कोटड़ा 21 2 9 7 7 - 25 2 नेवाण 7 - 1 - 2 - 3 3 बुजकंठा 8 - 1 1 - - 2 4 खडाल 19 8 10 - 2 - 20 5 विक्रमपुर 4 - - - - - - 6 फलौदी 10 8 14 1 4 - 27 7 पोकरण 15 13 5 7 11 - 36 8 कोरणावटी 12 5 4 13 3 1 26 9 मालाणी 8 4 - 22 8 7 41 10 सेवाणची 10 4 - 21 17 5 47 11 गोडवाड 27 3 - 3 4 1 11 12 बीकानेर 7 3 4 - 6 - 13 # योग 148 50 48 75 64 14 251 इस प्रसंग में कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। देवली उस शिला को कहते हैं जिस पर स्मारक को बनवाने वाले का नाम, जाति इत्यादि लिखा रहता है।
जो व्यक्ति किसी प्रकार की लड़ाई में जूझकर मरते हैं उनके स्मारकों को जुझार कहते हैं।
जो व्यक्ति राजा के अनुचित व्यवहार, राजकर्मचारियों का अन्याय असह्य हो जाने से सत्याग्रह करके अनशन द्वारा या और किसी प्रकार के हथियार से अपना प्राण विसर्जन कर देते हैं उनके स्मारकों को झोंवर कहते हैं।
जो स्त्री अपने पति के स्वर्गवास हो जाने पर उसके शव के साथ स्वयं भी चिता में जलकर मर जाती है उसे सती कहते हैं। उसके स्मारक को ही यहाँ सती कहा गया है।
मृत व्यक्ति की याद में जो छतरीनुमा स्मारक बनाते हैं उसे छतरी कहते है। जो केवल चबूतरे की आकृति का स्मारक होता है उसे चबूतरा कहते हैं। छतरी चबूतरे की अपेक्षा भव्य होती है।
-
अब शिलालेखों के विषय में कुछ विवरण प्रस्तुत हैं।
-
कोटड़ा छेड़
इस छेड़ के 21 ग्रामों में विक्रमी संवत् 1507 से 1901 तक के शिलालेख पाए जाते हैं। सबसे पुराना लेख नेगडरों गांव का विक्रमी संवत् 1507 का है। अन्य प्राचीन गांव साण्डा, रौंडी तथा सांधू है। तीन गांव मतीरो गोल, डांगरी और राजडावल से शिलालेख एकत्रित नहीं हुए।
तालाब / कूप
इस छेड़ के 5 गांवों (सांधू, खोडाल, बौंडा, जसेरो और काठोड़ा) में 7 तालाब बनवाने के लेख मिलते हैं। बीजोराई में ही दो कूप के शिलालेख हैं।
मन्दिर
दो गांवों (गूंगा एवं दईकोट) में मन्दिरों के शिलालेख हैं। -
नेवाण छेड़
इसमें 7 गांवों के शिलालेख संवत् 1566 से 1904 तक के मिलते हैं। संवत् 1566 का शिलालेख गरेरा ग्राम में देवली का है जिसमें मृत्यु के समय मेष लग्न तक का वर्णन है। यथा 'संवत् 1566 माघ सुदी 14 रविवारे पुष्य नक्षत्रे कर्कस्थ चंद्रे मेष लग्ने ब्रा. पिथड़ सुत हरी धवल सर्गे (स्वर्गे) गतः'। धनुवा में एक तालाब का शिलालेख है।
-
बुजकंठा छेड़
इसमें 8 गांवों के शिलालेख संवत् 1624 से 1882 तक के मिलते हैं। संवत् 1624 का शिलालेख रिद्ध गांव के तालाब का है जो उसकी प्राचीनता सिद्ध करता है। दो गांव मूणपिया तथा कंवरा से शिलालेख लिपिबद्ध नहीं किए गएरा
-
खडाल छेड़
इस छेड़ में 19 गांवों के शिलालेख संवत् 1471 से 1875 तक के मिलते हैं। नेडाई प्राचीनतम ग्राम है जिसमें तालाब का शिलालेख संवत् 1471 का है।
मन्दिर
आठ गांवों (नेडाई, खींया, मुन्धा, धामट, हड्डा, आसदे, माधो और काठोड़ी) में आठ मंदिरों के शिलालेख हैं।
तालाब/कूप
पांच गांवों (नेडाई, मुन्धा, रत्ता, घड़िया और चौधरी) में 8 तालाबों के शिलालेख मिलते हैं।
स्त्रींया एवं रत्ता में एक-एक कूप के शिलालेख हैं। -
विक्रमपुर छेड़
इस छेड़ का प्राचीन गांव बाप है जो विक्रम की 15वीं शताब्दी के परार्ध कालका है। इसमें ही पालीवालों के प्रसिद्ध देव क्षेत्रपाल है। भाद्रपद मास में क्षेत्रपाल का एक मेला भी यहां लगता है। पं. शिव नारायण जी ने 'पालीवाल इतिहास' में लिखा है कि 'यहां पालीवालों के बनाए हुए 2 मंदिर 2 कए, 4 छतरियां, 3 तालाब, और 8-10 देवलियां हैं।' परन्तु 'शिलालेख संग्रह' में इसका वर्णन नहीं। वहां जिन चार गांवों का वर्णन है उसमें संवत् 1618 से संवत् 1956 तक के शिलालेख मिलते हैं जिनके आधार पर भोजा की बाप पुराना गांव है जिसे भोजा नामक पालीवाल ने बाप के समीप ही बसाया था।
-
फलौदी छेड़
इस छेड़ के 10 गांवों में संवत् 1510 से 1976 तक के शिलालेख पाए जाते हैं जिनके आधार पर चार गांव जालोड़ा, होपारड़ी, मोखेरी एवं सावरीज प्राचीन सिद्ध होते हैं। जालोड़ा के एक तालाब का शिलालेख संवत् 1510 का है।
मन्दिर
सात गांवों में आठ मन्दिरों के शिलालेख हैं। सावरीज में 2 मन्दिर हैं। होपारड़ी, बिटड़ी, दयाकोर, जालोड़ा, भोजाकोर एवं गोदड़ली में एक - एक है। (इस संदर्भ में सावरीज के मन्दिर का विक्रमी संवत् 1700 का शिलालेख महत्त्वपूर्ण है जो हमारे वेद और शाखा पर प्रकाश डालता है। 'सावरंज ग्रामें पालीवाल धामट वंशे मुदगल गोत्रे मरूधनी शाखा जजुरवेद'.....इसमें मरूधनी शब्द माध्यन्दिनीय का अपभ्रंश शब्द है और जजुरवेद का शुद्धरूप यजुर्वेद है। पालीवाल ब्राह्मणों का वेद शुक्ल यजुर्वेद है। इनकी शाखा माध्यन्दिनीय है)।
तालाब
पांच गांवों में 7 तालाबों के शिलालेख हैं। जालोड़ा तथा सावरीज में 2-2 तालाब हैं। होपारड़ी, मोखेरी एवं निन्नेऊ में एक-एक है।
कूप
छः गांवों में 7 कूप के शिलालेख हैं। बिटड़ी में दो कूप, होपारडी, सावरीज, दयाकोर, गोदडली एवं भोजाकोर में एक-एक बनाए गए। -
पोकरण छेड़
इस छेड के 15 गांवों में संवत् 1622 से संवत् 1957 तक के शिलालेख हैं। सबसे प्राचीन शिलालेख लऊवाँ में संवत् 1622 का है। दूसरा ढदू का संवत् 1688 का है। इस छेड़ के ये ही प्राचीन गांव है।
तालाब/कूप
उगरास मुन्धा में एक तालाब तथा एक कूप का शिलालेख है। फलसूंड में भी एक कूप है। एक बावड़ी मावा निवासी ने 'रामडेरा' में बनवाई दूसरी लऊंवा में है।
मन्दिर
इस छेड़ में सर्वाधिक 13 मंदिरों के शिलालेख 9 गांवों में मिलते हैं। लऊवाँ में 3, ढढू तथा धूलसर में 22 हैं। एक-एक मंदिर मडला बड़ा, मडला छोटा, चांसवा, मावा, उगरास कर्माणी तथा फलसूंड में है। -
कोरणावटी छेड़
इस छेड़ के 12 गांवों में पाए गए शिलालेखों का समय संवत् 1570 से संवत् 1982 तक का है। इसके प्राचीन गांव बाबड़ली और लोरड़ी हैं।
मन्दिर
चार गांवों में 5 मंदिर है। दो मन्दिर गंगावा में, एक - एक रोड़वा, बावड़ली तथा लोरड़ी में है।
तालाब/कूप
एक-एक तालाब बावडली तथा कई में है। एक कुआं लोरडी में तया दूसरा रोड़वा में है। -
मालाणी छेड़
इस छेड़ के 8 गांवों में संवत् 1585 से संवत् 1949 तक के शिलालेख पाए जाते हैं। इसमें सरली, तलवाड़ा और जेरडा प्राचीन गांव है।
मन्दिर
तीन गांवों में 4 मन्दिर हैं। एक सरली में, दो जसोल में तथा एक तेमावास में है। -
सेवाणची छेड़
इस छेड़ के 10 गांवों में संवत् 1610 से 1986 तक के शिलालेख पाए जाते हैं। बीठूजा और रामीण प्राचीन गांव हैं।
मन्दिर
तीन गांवों में 4 मंदिर हैं। दो मन्दिर बालोत्तरा में, एक-एक मड़ापड़ा तथा मूंगड़ा में है। -
गोड़वाड छेड़
इसके 27 गांवों में संवत् 1622 से 1981 तक के शिलालेख मिलते हैं। सबसे प्राचीन शिलालेख खारावेरा भींवतो का संवत् 1622 का है।
मन्दिर
तीन गांवों में 3 मन्दिर हैं। खांवल, वणियावास तथा जाजियाल में एक-एक मंदिर है। -
बीकानेर छेड़
इसके 7 गांवों में संवत् 1703 से 1937 तक के शिलालेख मिलते हैं। अज्जु सबसे प्राचीन गांव है।
मन्दिर
दो गांवों में 3 मन्दिर हैं। दो चानी में तथा एक कोलायत जी में है।
तालाब/कूप
एक कुआं चांडासर में तथा दो झज्जू में हैं। एक तालाब भायला में है।
इन शिलालेखों से हमारी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।
धार्मिक कार्य
पालीवालों के ओला - स्थित यज्ञ-स्तंभ एवं दस उजाणे की चौकियां इस बात का प्रबल प्रमाण है कि हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के यजन कर्म को अत्यंत श्रद्धापूर्वक करते थे। काकेलाव में 3 चौकी, बणियावास में 2 तथा खांवल, बिचपड़, झींतडा, निम्बाड़ा और तलवाड़ा में एक- एक है। सबसे प्राचीन चौकी बणियावास में संवत् 1874 की है।
इनके द्वारा निर्मित 50 मन्दिर भी बता रहे हैं कि इन्हें मन्दिर निर्माण कराने में अत्यंत रूचि थी। 'इष्ट' कर्म में यज्ञ करना, मन्दिर निर्माण आते हैं। ये 50 मन्दिर 41 गांवों में है। लऊवाँ में 3 मन्दिर हैं। सात गांवों में दो-दो मन्दिर है। ये सात गांव सावरीज, ढढू, धूलसर, गंगावा, जसोल, बालोतरा एवं चानी हैं। शेष 33 गांवों में एक-एक मंदिर है। सबसे प्राचीन मन्दिर सरली में संवत् 1668 का है।
वेद, शारवा
दो शिलालेख वेद और शारवा संबंधी भी है। पहला सावरीज (फलौदी) के मंदिर में संवत् 1700 का है जिसमें 'जजुरवेद' और 'मरूध नी' शाखा कही है। दूसरा ढढू (पोकरण) की छतरी का संवत् 1709 का है। इसमें 'माधनीक शाख' और 'जजरवेद' लिखा है। 'जजरवेद' यजुर्वेद का अपभ्रंश है और 'माधनीक शास्व', अरुधनी शारवा' माध्यन्दिनीय शाखा के अपभ्रंश हैं। हमारा वेद शुक्ल यजुर्वेद तथा शाखा 'माध्यन्दिनीय' है।
तालाब, कुआ, बाबड़ी निर्माण
पालीवालों द्वारा निर्मित 48 तालाब, कुआं आदि बता रहे हैं कि इन्हें पुराणों में वर्णित 'पूर्त' कर्म में कितनी श्रद्धा थी। इस प्रकार इनकी 'इष्टापूर्त' कर्मा की साक्षी अभी तक वर्तमान है। इनमें 18 कूप 15 गांवों में है। तीन गांव बीजोराई, बिटडी एवं झज्जू में 22 कूप हैं। बीजोराई में प्राचीनतम कूप संवत् 1657 का है। इनके 28 तालाब 21 गांवों में है। सात गांवों में दो-दो तालाब हैं। ये सात गांव बौंडा, जसेरो, नेडाई, रत्ता, चौधरी, जालोड़ा और सावरीज हैं। प्राचीनतम शिलालेख नेडाई के तालाब का संवत् 1471 का है। एक-एक बावड़ी लऊवाँ तथा रामडेरा में है।
आर्थिक स्थिति
इनके बनाए भव्य मकान (कुलधर की हवेलियां), धर्मशाला, मन्दिर, कुआं, बावड़ी, आदि इस बात के प्रमाण हैं कि इनके पास धन था जो इन्होंने अपने पुरुषार्थ से पाली पतन के बाद कमाया था। एक - एक धर्मशाला लोरड़ी, खांवल एवं बालोतरा में है। लोरड़ी की धर्मशाला संवत् 1885 की है।
सती प्रथा
इनके 75 सती स्मारक बतला रहे हैं कि हमारे समाज में भी सती प्रथा चालू थी। इसका अधिक प्रभाव मालाणी, सिवाना तथा कोरणावटी में था जहां क्रमशः 22, 21, 13 सती स्मारक हैं।
युद्धों में सहयोग
व्यापार तथा वणिज प्रधान जाति युद्ध प्रिय तो नहीं होती फिर भी इनके 64 जुझार स्मारक बता रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इन्होंने क्षात्र धर्म का भी पालन किया है।
-
कोटड़ा छेड़
( यह लेख “पालीवाल ब्राह्मण” किताब, लेखक श्री ओमप्रकाश पालीवाल I.E.S(Retd.)(M.A. LLB) ३२७८ सेक्टर 15D Chandigarh द्वारा मार्च २००५ को प्रकाशित )
परिचय पत्र - ऑनलाइन पंजीकरण
परिचय ऑनलाइन पंजीकरण एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे समुदाय के सदस्यों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म उन व्यक्तियों को सुरक्षित तरीके से अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर जानकारी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा देता है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सुलभ और काग़ज़ रहित हो जाती है। चाहे बात विवाह संबंधी जानकारी की हो, समुदायिक रिकॉर्ड की, या किसी आयोजन में भाग लेने की — परिचय ऑनलाइन पंजीकरण यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के सदस्य अपने घर बैठे, कंप्यूटर या स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकें।
शुरुआत करें